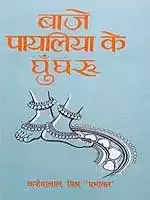|
कहानी संग्रह >> बाजे पायलियाँ के घुँघरू बाजे पायलियाँ के घुँघरूकन्हैयालाल मिश्र
|
335 पाठक हैं |
||||||
सहज, सरस संस्मरणात्मक शैली में लिखी गयी प्रभाकर जी की रचना बाजे पायलियाँ के घुँघरू।
मैं पशुओं में हूँ, पशु-जैसा ही हूँ पर पशु नहीं हूँ !
जिज्ञासा :
स्वतन्त्र भारत के केन्द्रीय शासन-द्वारा आयोजित साहित्य-संस्कृति-संगम का उद्घाटन दिल्ली के लाल क़िले में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हो चुका तो प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू संस्कृति पर बोलने को माइक पर आये।
उनके भाषण का पहला वाक्य लगभग यह था, “आप जानते हैं कि मुझे तो संस्कृति-कल्चर के मामलों में बहुत दिलचस्पी है, पर मुसीबत तो यह है कि इस मसले पर मैं ज्यों-ज्यों गौर करता हूँ, आलिमों-विद्वानों से मिलता हूँ या उनकी किताबें पढ़ता हूँ, उलझता जाता हूँ।"
नेहरू का यह वाक्य सुनकर मैं अपने में ऐसा उलझ गया कि मुझे नहीं मालूम फिर आगे उन्होंने क्या कहा। सहसा मुझे याद आ गयी अपने ही जीवन की एक घटना। मेरे नगर का विशाल तालाब है देवीकुण्ड। उसमें तैरते-डुबकियाँ लेते मैं पला-पनपा, पर उस दिन तैरते-तैरते कमल-वन में जा घुसा तो लगा कि अब लौटना असम्भव है।
हाथों और पैरों में कमल की नालें इस तरह लिपटी कि एक से छू, तो दो में उलझू और दो से छुटूं तो चार में और बस छूटने-उलझने की कशम-कश में हालत यह हो गयी कि मकड़ी के मायाजाल में फँसी मक्खी से मैं अपनी उपमा दे सकूँ। अपने प्रिय नेहरू की उलझन मुझ पर कुछ इस तरह छा गयी कि लगा मैं इस समय भी उसी कमल-वन में उलझा हुआ हूँ।
नेहरू के बाद आसफ़अली आये और उन्होंने विनय को ही संस्कृति कहा तो काका कालेलकर ने संस्कृति के नाम पर शुद्धि, समृद्धि, सामर्थ्यऔर समाधान की चर्चा की और इस तरह दो दिनों तक वर्चस्वी विद्वानों के भाषण सुनकर सचमुच स्वयं मेरी भी हालत नेहरू-जैसी ही हो गयी कि कहूँ, “पर मुसीबत तो यह है कि मैं इस मसले पर ज्यों-ज्यों गौर करता हूँ, आलिमों-विद्वानों से मिलता हूँ या उनकी बातें सुनता हूँ, उलझता जाता हूँ।"
सोचा, आखिर यह संस्कृति है क्या कि जिसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, पर मानव की अनिवार्यता होकर भी वह ऐसा गूढ़ तत्त्व कि उसकी आँख-पूँछ तो हरेक देखता है, पर उसकी पूर्णता के दर्शन, उसका स्पष्ट ज्ञान, किसी को भी सुलभ नहीं?
अजीब उलझन है और उलझन का तक़ाज़ा है कि उसे सुलझाया जाए, पर यह सुलझे कैसे? उलझन को सुलझाने का मेरा अपना तरीक़ा यह है कि जब सुलझाते-सुलझाते बुद्धि उलझने लगे तो मैं उसे अपने अन्तर्यामी को सौंपकर सो जाता हूँ। बस संस्कृति की उलझन भी मैंने अपने अन्तर्यामी को सौंपी और निश्चिन्त हो गया।
कोई चौदह महीने बाद देवप्रयाग के पर्वतों की गोद में अलखनन्दा और गंगा के संगम पर बैठे-बैठे मुझे अन्तर्यामी के बोल सुनाई पड़े। नम्र हो, मैंने उन्हें भाषा में बाँध लिया।
|
|||||
- उग-उभरती पीढ़ियों के हाथों में
- यह क्या पढ़ रहे हैं आप?
- यह किसका सिनेमा है?
- मैं आँख फोड़कर चलूँ या आप बोतल न रखें?
- छोटी कैची की एक ही लपलपी में !
- यह सड़क बोलती है !
- धूप-बत्ती : बुझी, जली !
- सहो मत, तोड़ फेंको !
- मैं भी लड़ा, तुम भी लड़े, पर जीता कौन?
- जी, वे घर में नहीं हैं !
- झेंपो मत, रस लो !
- पाप के चार हथियार !
- जब मैं पंचायत में पहली बार सफल हुआ !
- मैं पशुओं में हूँ, पशु-जैसा ही हूँ पर पशु नहीं हूँ !
- जब हम सिर्फ एक इकन्नी बचाते हैं
- चिड़िया, भैंसा और बछिया
- पाँच सौ छह सौ क्या?
- बिड़ला-मन्दिर देखने चलोगे?
- छोटा-सा पानदान, नन्हा-सा ताला
- शरद् पूर्णिमा की खिलखिलाती रात में !
- गरम ख़त : ठण्डा जवाब !
- जब उन्होंने तालियाँ बजा दी !
- उस बेवकूफ़ ने जब मुझे दाद दी !
- रहो खाट पर सोय !
- जब मैंने नया पोस्टर पढ़ा !
- अजी, क्या रखा है इन बातों में !
- बेईमान का ईमान, हिंसक की अहिंसा और चोर का दान !
- सीता और मीरा !
- मेरे मित्र की खोटी अठन्नी !
- एक था पेड़ और एक था ठूंठ !
- लीजिए, आदमी बनिए !
- अजी, होना-हवाना क्या है?
- अधूरा कभी नहीं, पूरा और पूरी तरह !
- दुनिया दुखों का घर है !
- बल-बहादुरी : एक चिन्तन
- पुण्य पर्वत की उस पिकनिक में